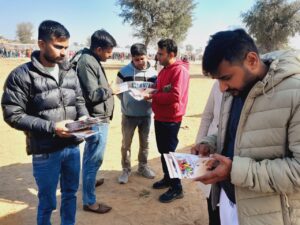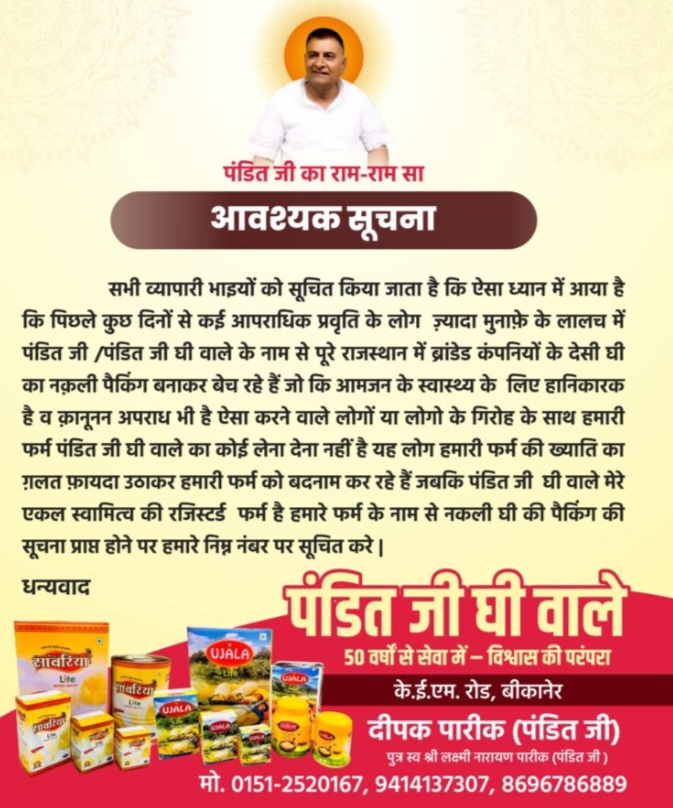



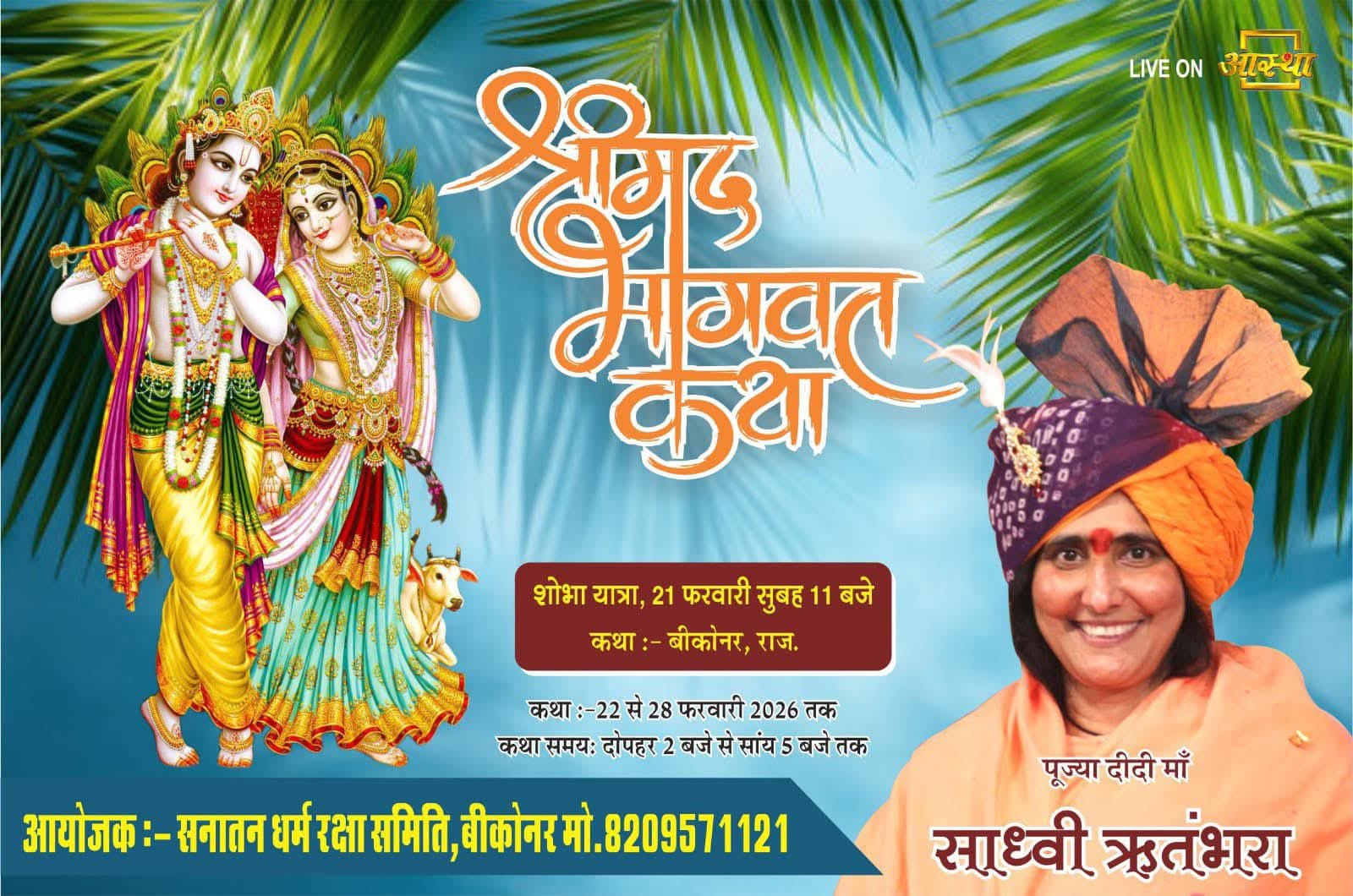



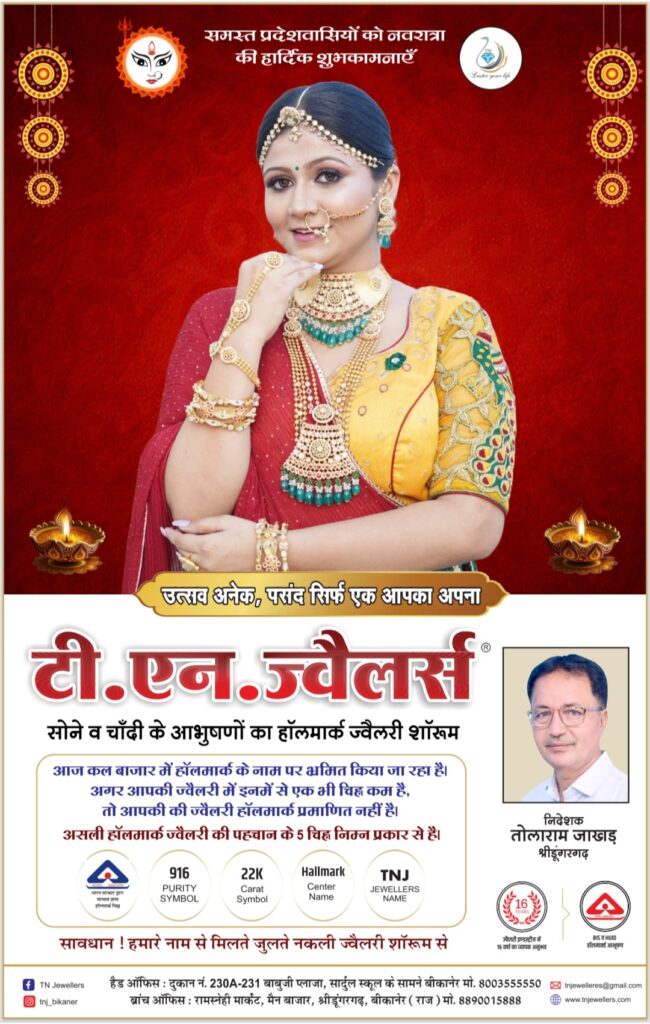

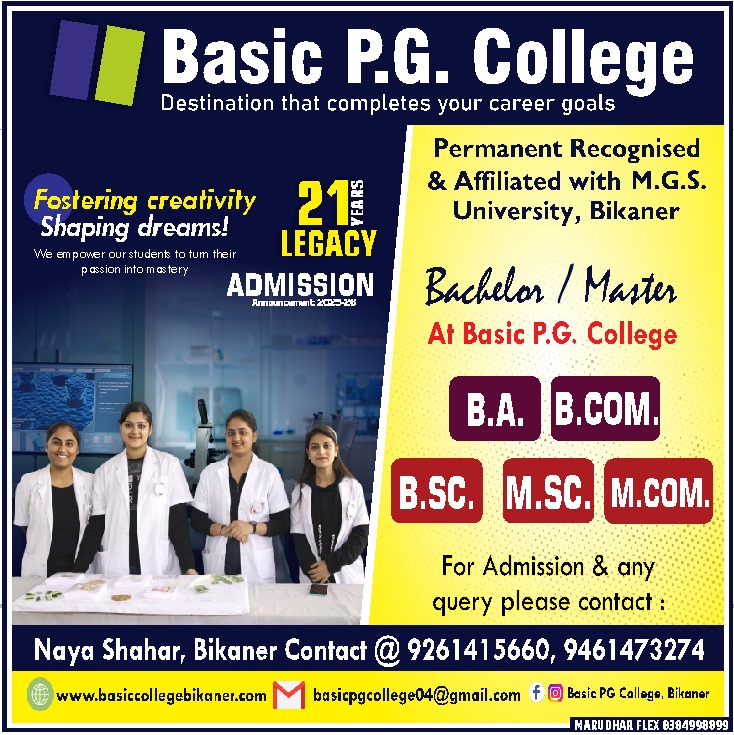
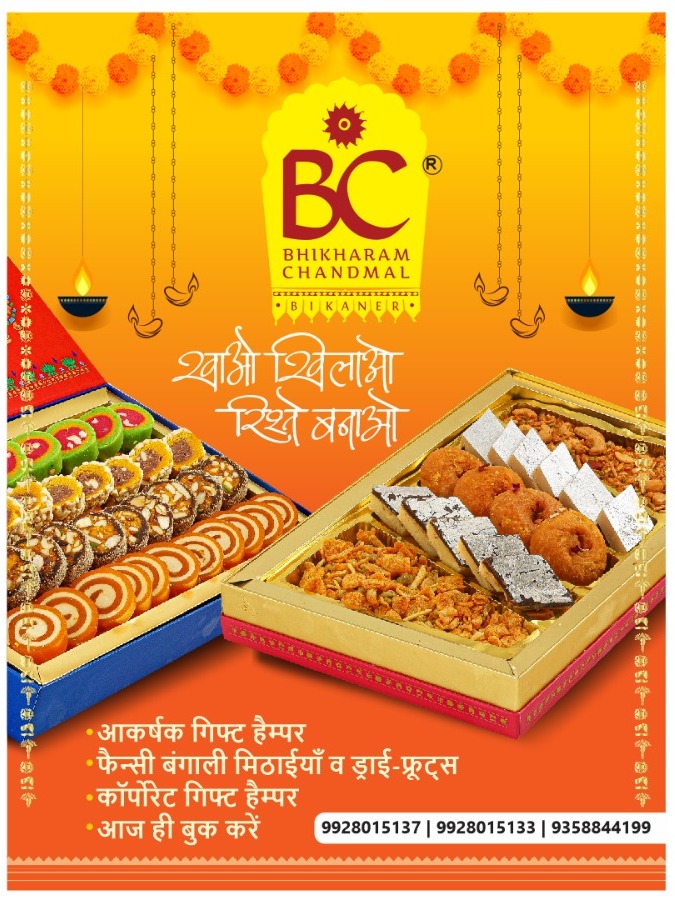

बीकानेर,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना को सौ साल का हो चुके हैं। 17 अक्टूबर 1920 को तात्कालिक सोवियत रूस आज के उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में मानवेन्द्रनाथ रॉय (एमएन रॉय) ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। तब देश का नाम ‘इंडिया’ पार्टी के हु नाम के शुरु या अंत में रखने पर भी लम्बी बहस चली। निर्णय कम्युनिस्ट इन्टरनेशनल के हस्तक्षेप से इंडिया नाम अंत में लगा और नाम मिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया।
इससे पहले भी एमएन रॉय ‘सोशलिस्ट वर्क्स पार्टी’ बना चुके थे। भाकपा की स्थापना के बाद रॉय ने स्वयं वामपंथ विचार को सिरे से नकार दिया और रेडिकल ह्यूमनिज्म (वैज्ञानिक मानववाद) की नई अवधारणा दे डाली। हालांकि आधिकारिक रूप से भारत में भाकपा का विधिवत् गठन 26 दिसम्बर 1925 को कानपुर में हुआ। तत्पश्चात 1933 में भाकपा का पुनर्गठन हुआ।
स्थापना के साथ ही भाकपा को कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में सक्रियता से किसान-मजदूर की पार्टी के रूप में पहचान मिली। संगठन ने जल, जंगल और जमीन के लिए सुदूर क्षेत्रों में संघर्ष किए। जिससे आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो गए। पश्चिम बंगाल में तेभागा आंदोलन, पुन्नया वलयार किसान आंदोलन, आंध्रप्रदेश के तेलंगाना में सशस्त्र किसान आंदोलन से निजाम के अधिकार से तीन हजार गांव मुक्त करवाए। भूमि को जोत के आधार पर बांटने के निर्णय ने जन मानस में वामपंथ को संघर्ष का रोल मॉडल बनाने में अहम भूमिका निभाई। वामपंथी तत्कालीन राजे-रजवाड़ों, सामंतवादी सेठ-साहूकारों से भी लड़ते-भिड़ते रहे। परन्तु उन्होंने भारतीय समाज की धूरी रही जाति व्यवस्था’ को कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया। दलित और आदिवासी समुदायों में राजनीतिक सेंध लगाने की वामपंथ की कयावद प्रारम्भ से
ही जारी है। अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों एवं आन्तरिक अर्न्तद्वंद के चलते सन् 1964 में वामपंथ को बड़ा झटका लगा, जब चीन आक्रमण के बाद भारतीय वामपंथियों की राष्ट्रीय निष्ठा और अंतरराष्ट्रीय निष्ठा के बीच संघर्ष हुआ। भाकपा में विभाजन स्वरूप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ।
वामपंथ में कई वैचारिक दरारों न के चलते भाकपा माले, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी वामपंथी दलों का भी उदय हुआ। हालांकि बाद में वाममोर्चा की छतरी के नीचे फिर से संगठित होने का प्रयास भी हुआ। परन्तु वैचारिक – संघर्ष बना रहा। इसके साथ ही • नक्सली वामपंथ के साथ भी अन्य वामपंथी दलों का साध्य और साधन को लेकर बड़ा वैचारिक संघर्ष रहा। गौरवपूर्ण संसदीय इतिहास का
अध्ययन करने पर वामपंथी विचार और नेताओं का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। परन्तु यह चिरस्थाई नहीं रह सका। सदन की बहसों, शून्यकाल, अनुदान मांगो, बजट भाषणों, विधेयक चर्चा के अलावा विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में कानूनों के निर्माण में वामनेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
एमएन. राय, मोहम्मद अली, मोहम्मद सफीक सिद्दीकी, अबनी मुखर्जी, एसए डांगे, पीसी जोशी, बीटी रणदेवे, अजय घोष, हीरेन मुखर्जी, एबी वर्धन, ईएमएस. नम्बुदरीपाद, ज्योति बसु, हरिकिशन सिंह सुरजीत, सोमनाथ चटर्जी, चतुरानन मिश्र, इन्द्रजीत गुप्त, सीताराम येचुरी, हन्नान मौला, प्रकाश कारात, वृंदा करात सरीखे राष्ट्रीय नेताओं के साथ सांसद श्योपत सिंह मक्कासर, कॉ. हेतराम बेनिवाल, कॉ. अमराराम सूबे, पवन दुग्गल, बलवान पूनिया, गिरधारीलाल महिया आज के संघर्षशील नेताओं में शुमार है। ‘इन्होंने संसद व विधानसभा में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवाई। भूमि सुधार, श्रम कानून, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन, कार्य की तय अवधि, सामाजिक सुरक्षा योजना, कर्मचारियों हेतु पेंशन प्रावधान, न्युनतम वेतन, प्रशासकीय सुधार, निजीकरण का विरोध, सीमांत व लघु कृषकों के अधिकार, बैंकिंग प्रणाली सुधार खाद्यान्न, डीजल-पेट्रोल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए शासन को मजबूर किया है। यह तथ्य केन्द्र सरकार की ओर से तीन किसान बिलों को वापस लेने से स्वयं सिद्ध होती है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के संघर्ष को लम्बा चलाने में कम्यूनिस्ट नेताओं की धरातल पर रही भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।